*’पेयजल’ लेखक उमेश बाली*



पेयजल
भारत के हर शहर हर गांव की समस्या है पीने का पानी। हर जगह कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बहुत भारी समस्या है और आज भी महिलाओ को सर पर उठा कर लाना पड़ रहा है । दूसरी समस्या जहां पानी मिल भी रहा है अधिकतर इलाकों में वो सीधा पीने के काबिल नही । पानी को शुद्ध करने के प्लांट पुरानी तकनीक के हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं कि पानी जनित रोगों को रोका जाय । हर आदमी गैस या पेट खराब की शिकायत करता है । घरों में फिल्टर और ro लगाने पड़ रहे हैं । बरसात में और भी बुरी हालत। ऐसा कोई प्लांट मेरी निगाह में नही जो गंदले पानी को पूरी तरह साफ़ कर सके । पुराने तरीके से हवा निकालने के लिए किए गए सुराख जब पानी होता है तो बरबाद होता है और जब नही होता तो बाहरी गंदा पानी कई जगह भीतर प्रवेश कर जाता है । कई स्थानों पर बरसो पुरानी लाइनें हैं जहां पानी रिसता रहता है एक पहलू तो यह है । दूसरा पहलू करीब हर गांव या कसबे में कुछ घर जिन्हे विभाग अपनी भाषा में tale कहता है पानी नही पहुंचता । वास्त्व में पानी के लिए कोई योजना दिखाई नही देती । hit n trial पद्धति अपनाई जाती है । एक पाइप जो 30 घरों के लिए थी उस पर 100 से अधिक आश्रित हो जाते हैं । हर साल नए घर बनते हैं और पानी वही। एक जो कमी मुझे दिखाई देती है बिना पानी के स्रोत की क्षमता मापे नई योजनाएं , टैंक , या पाइप लाइन बिछा दिए जाते हैं । बाद में फिर वो ही दो चार दिन किसी का कम कर दो दो चार का बढ़ा दो विभाग के प्लंबर लोगो की कोई सुनता नही विभाग अपने से कुछ ठोस करने को अधिकृत नही बार बार जाओ तो मंत्री से बात करो । और यह भी विडम्बना है कि जो काम विभाग को करना चाहीए इसके लिए विधायक या मंत्री के पास जाना पड़ता है । सबसे बडा जो दोष देखा गया वो जल प्रबंधन की कमी है और विभाग के पास आज भी साधनों की कमी है विशेषकर मानव शक्ति की और दूसरी सामान की कमी । तीसरी योजना का सही न होना । इस समस्या का तीसरा पहलू है जल की बरबादी । अक्सर सार्वजनिक नल तो लोग खुले छोड़ते ही हैं घरों में यही हाल है । कई जगह पानी के मीटर नही है जो बर्बादी का कारण बनता है ।मैने ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान देखा है कि विभाग को यह मालूम होता है एक परिवार को संख्या के हिसाब से अधिकतम कितना पानी चाहीए और उसका डिस्चार्ज कितना होना चाहिए । पाइप की मोटाई , पानी की गति और पानी का दवाब सब माप कर यानि calculated , कोई ro की जरूरत नहीं कोई फिल्टर की जरूरत नहीं । इतने शानदार आइसोलेटेड प्लांट की मैं देख कर दंग रह गया आधुनिक मशीनें यहां तक की क्लोरीन भी माप कर छोड़ी जाती है । विभागीय चौकसी इतनी की कोई मक्खी भी कैसे घुस जाए । अगर कभी कोई पानी जनित रोग पैदा हो जाए तो स्वास्थ्य विभाग जांच की सिफारिश करता है और दिनों में नही घंटो में कार्यवाही शुरू हो जाती है वहां के नेता यह नही कहते की दोषी बक्शे नही जायेंगे करवाही होती है नतीजे लेकर ।पानी का प्रबंध ऐसा है कि बर्बादी का चांस नहीं छोड़ा । पानी की बरबादी हो ही नही सकती । जीतना परिवार को पानी चाहीए उतना मिलता है । लेकिन जितना पानी मिलता है और अगर उससे अधिक उपभोग बढ़ जाए तो नोटिस इश्यू होता है कि आप का उपभोग बढ़ गया है क्यों? अगर उपभोक्ता का उत्तर संतोष जनक नही होता तो जुर्माना भी और पानी का रेट भी बढ़ेगा । अगर किसी वजह से पानी अवरुद्ध होता है तो आपको पानी उपलब्ध करवाया ही जायेगा और पानी की टंकी में दिया जायेगा आपकों खुद नही लाइन में लगना । इसे कहते हैं पानी का प्रबंधन । बरबादी के मामले में बेहद सावधान रहते हैं वहां के नागरिक। मैं हैरान होता हूं अपने नेता लोग वहां क्या समझ कर आते हैं ? यह होबार्ट में मैने देखा और महसूस किया ।वहां किसी भी कार्य के लिए जनता को विधायक या मंत्री के पास जानें की अवश्यकता नही पड़ती अपितु सबंधित विभाग या कंपनिया जिम्मेदारी निभाती हैं । वहां हर एक को सुविधा बराबर , हर एक अधिकारों का सम्मान और हर एक अपने फर्ज को अंजाम देता है ।

धन्यवाद । उबाली ।
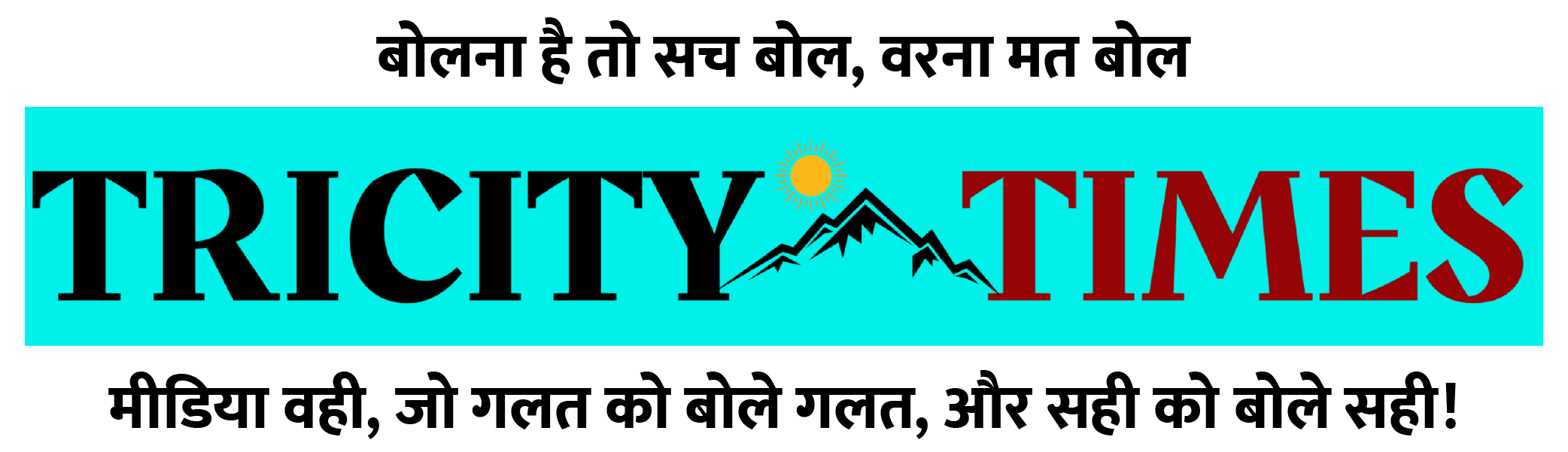




आपके द्वारा लिखा गया लेख को पढ़कर मन बहुत प्रभावित हुआ। इस तरह की प्रणाली यदि हिमाचल प्रदेश में भी अपनाई जाए दूर नहीं जब हिमाचल से औरों जैसे प्रोडक्ट गायब हो जाएंगे । जल ही जीवन के आधार पर लिखे गए लेख की जितनी तारीफ की जाए कम है मानना है कि एक बार अगर इस तरह के लेख को कोई पढ़ लेता है खुद बदलने की कोशिश जरूर करेगा क्योंकि जब तक किसी की आंख नहीं खुली जाती तब तक वे अनजाने में अंधापन का ड्रामा रचा रहता है इस प्रकार के लेख से प्रभावित होकर हम सबको मिलजुल कर आगे आना चाहिए जिससे कि एक तो पानी की कमी दूर होगी और दूसरे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा क्राइम इस तरह के लेख को पाठ्यक्रम के द्वारा सभी शिक्षक संस्थाओं में पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि शुरू से ही इस पर अमल लाया जा सके